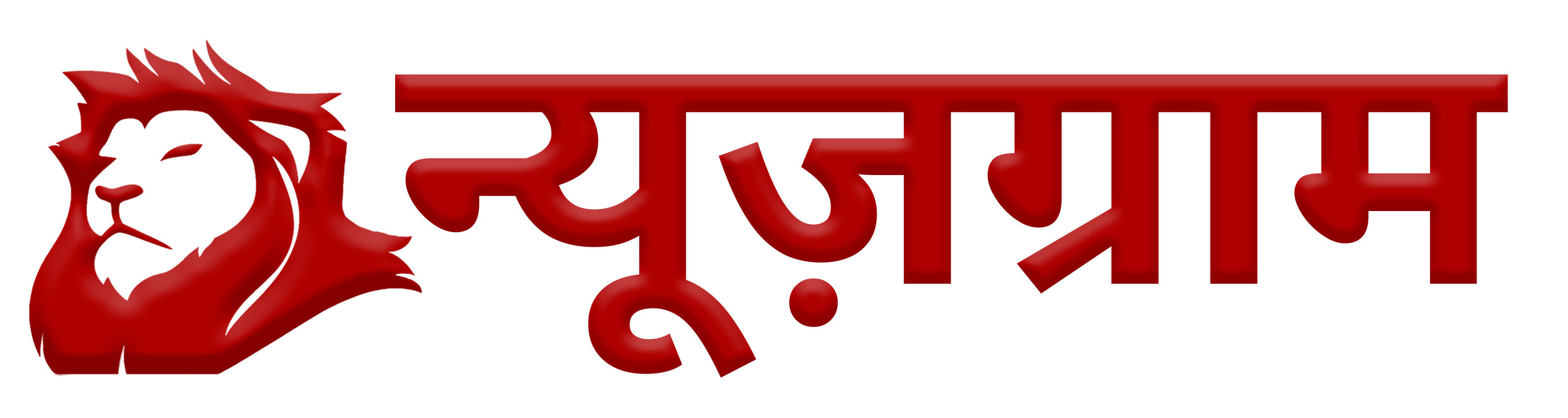1. हज़ारिबाग जेल से दिवाली पर फरारी: लोकनायक की साहसी छलांग
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन (Quit India Movement) के दौरान जयप्रकाश नारायण (JP) को हज़ारिबाग सेंट्रल जेल में बंद किया गया। 8 नवंबर 1942 की दिवाली की रात उन्होंने अपने साथियों के साथ फरार होने का साहसी निर्णय लिया। 56 धोती जोड़कर रस्सी बनाई गई और दीवार फांदकर बाहर निकलने का प्रयास किया गया। यह अभियान लगभग 9 घंटे चला और ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी संदेश बन गया। हालांकि उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन यह घटना आज़ादी की लड़ाई में JP की बहादुरी और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक मानी जाती है।
2. नेपाल के जंगलों में ‘आजाद दस्ता’ की कहानी
जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण नेपाल पहुंचे और वहाँ उन्होंने "आजाद दस्ता" ("Freedom Squad") नामक एक गुरिल्ला संगठन की नींव रखी। यह संगठन ब्रिटिश शासन के खिलाफ सक्रिय हुआ और नेपाल के जंगलों को अपना ठिकाना बनाया। JP ने यहां से स्वतंत्रता सेनानियों को संगठित करने और हथियारों की व्यवस्था करने का प्रयास किया। हालांकि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन "आजाद दस्ता" ने साबित किया कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल खुले आंदोलनों से नहीं बल्कि गुप्त संघर्ष और साहसिक रणनीतियों से भी लड़ी जा सकती है। यह उनकी क्रांतिकारी सोच और जोखिम उठाने की क्षमता को दर्शाता है।
3. विदेश से लौटा एक मार्क्सवादी विचारक
1922 में अमेरिका जाकर जयप्रकाश नारायण ने शिक्षा हासिल की। वहां रहते हुए वे मार्क्सवाद और समाजवाद की विचारधारा से गहराई से प्रभावित हुए। मजदूरों और गरीबों के संघर्ष ने उनके सोच को नया रूप दिया। 1929 में भारत लौटकर उन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी (Congress Socialist Party) के गठन में भूमिका निभाई। इस पार्टी का लक्ष्य कांग्रेस के भीतर वामपंथी धारा को मजबूत करना था। यह दौर उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं, बल्कि एक विचारक और समाज सुधारक भी बनाया। उनके समाजवादी दृष्टिकोण ने आगे उनके सभी आंदोलनों को दिशा दी।
4. विवाह, आश्रम और सत्याग्रह की अनोखी शुरुआत
JP ने 1920 में प्रभारवती देवी से विवाह किया। प्रभारवती देवी स्वयं गांधीजी के मार्गदर्शन में साबरमती आश्रम में रहीं और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ीं। विवाह के बाद भी दंपति ने निजी जीवन को आंदोलन के साथ जोड़ दिया। JP ने अपनी पढ़ाई और आरामदायक भविष्य छोड़कर आंदोलन की राह चुनी। उन्होंने असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह में भाग लिया। प्रभारवती देवी ने भी त्याग और समर्पण का जीवन अपनाया। इस प्रकार, विवाह उनके लिए व्यक्तिगत सुख की शुरुआत नहीं बल्कि राष्ट्रसेवा और सामाजिक परिवर्तन की अनोखी यात्रा का हिस्सा बना, जो जीवनभर जारी रहा।
5. भारत छोड़ो आंदोलन में बेमिसाल भूमिका
1942 का भारत छोड़ो आंदोलन (Quit India Movement) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक क्षण था। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण अग्रणी नेताओं में से एक बने। जेल में रहते हुए भी उन्होंने क्रांतिकारी योजनाएँ बनाई और जनता को प्रेरित किया। उनका संदेश साफ था "अंग्रेज़ों भारत छोड़ो।" इस दौरान उनकी गिरफ्तारी और बाद में जेल से भागने की कोशिश ने उन्हें जनता का सच्चा नायक बना दिया। वे केवल विरोधी भाषण नहीं देते थे, बल्कि जमीन पर सक्रिय रहकर जनता को आंदोलित करते थे। इस आंदोलन में उनकी भूमिका ने उन्हें "लोकनायक" के रूप में स्थापित कर दिया।
6. बिहार आंदोलन और सम्पूर्ण क्रांति का नारा
1974-75 में बिहार के छात्रों और युवाओं ने भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। इस आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। उन्होंने "सम्पूर्ण क्रांति" (Total Revolution) का नारा दिया। यह क्रांति केवल राजनीतिक बदलाव तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और नैतिक सुधार भी था। JP ने जनता से कहा कि बदलाव केवल चुनावों से नहीं आएगा, बल्कि हर व्यक्ति को समाज सुधार में योगदान देना होगा। यह आंदोलन आपातकाल की पृष्ठभूमि बना और JP को युवाओं का सच्चा नेता सिद्ध किया। उनका यह नारा आज भी प्रेरणा देता है।
7. कैद, बीमारी और डायलिसिस के बावजूद संघर्षरत JP
आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया। उसी समय उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें गंभीर किडनी की बीमारी का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी किडनी हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो चुकी है और उन्हें जीवनभर डायलिसिस की जरूरत होगी। इसके बावजूद JP ने अपने संघर्ष को नहीं छोड़ा। उन्होंने जेल से भी जनता को प्रेरित किया और लोकतंत्र की बहाली के लिए आवाज बुलंद की। बीमारी ने उनके शरीर को कमजोर किया, लेकिन उनकी विचारधारा और जज़्बा आज़ादी और लोकतंत्र की मशाल बने रहे।
8. विभाजन और दंगों के बीच अमन का संदेश
1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब विभाजन की त्रासदी ने पूरे देश को हिला दिया। लाखों लोग विस्थापित हुए और सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। इस कठिन दौर में जयप्रकाश नारायण बिहार लौटे और वहाँ दंगों को रोकने की कोशिश की। उन्होंने शांति समितियों का गठन किया और लोगों से अमन बनाए रखने की अपील की। उनका मानना था कि आज़ादी का सही अर्थ तभी है जब लोग एक-दूसरे के साथ भाईचारे से रहें। विभाजन के दौरान JP की सक्रियता ने दिखाया कि वे केवल राजनीति नहीं बल्कि मानवता और शांति को सर्वोपरि मानते थे।
9. सत्ता से दूरी, सेवा से नाता: भूदान आंदोलन में JP
1948 में कांग्रेस से अलग होने के बाद JP ने पार्टी राजनीति से दूरी बना ली। उन्होंने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से खुद को जोड़ा। यह आंदोलन ज़मीनहीनों को ज़मीन दिलाने के लिए शुरू किया गया था। JP ने गाँव-गाँव जाकर इस आंदोलन को गति दी और किसानों तथा भूमिहीनों के बीच काम किया। इससे साबित हुआ कि उनके लिए सत्ता की राजनीति मायने नहीं रखती थी, बल्कि जनता की सेवा ही उनका सच्चा उद्देश्य था। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह सामाजिक सुधार और जनता की भलाई के लिए समर्पित कर दिया।
10. आपातकाल और इंदिरा गांधी को ठुकराया दान
आपातकाल (1975-77) के दौरान जब जयप्रकाश नारायण की सेहत बहुत बिगड़ गई, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनकी चिकित्सा सहायता के लिए ₹90,000 का दान देने की पेशकश की। लेकिन JP ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे बड़े दान नहीं चाहते, बल्कि जनता की छोटी-छोटी मदद से ही जीना चाहते हैं। यह कदम उनकी निष्ठा और सादगी का प्रतीक था। उन्होंने दिखाया कि लोकतंत्र और नैतिकता उनके लिए व्यक्तिगत लाभ या राजनीतिक सौदेबाजी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। यह प्रसंग उनके व्यक्तित्व की महानता को उजागर करता है। [Rh/SP]